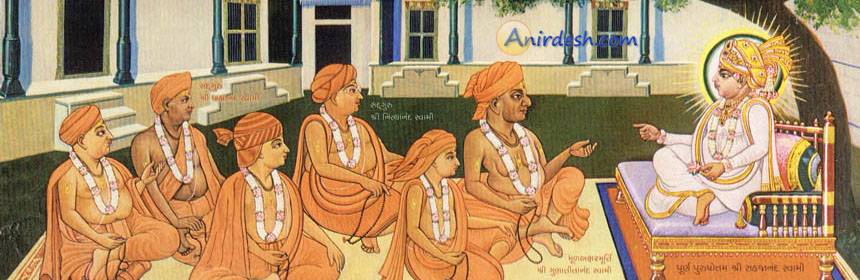ટીપણી
પ્રકરણ: ગઢડા પ્રથમ, સારંગપુર, કારિયાણી, લોયા, પંચાળા, ગઢડા મધ્ય, વરતાલ, અમદાવાદ, ગઢડા અંત્ય, ભૂગોળ-ખગોળ, વધારાનાં
| Id | Vach | No | Footnote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | १. पुत्र-धनादि। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | २. ‘धर्मकुल’ से श्रीहरि का अभिप्राय धर्मपिता-भक्तिमाता के कुल से नहीं है, अपितु ‘धर्मकुल’ का अर्थ यहाँ पर स्वयं ‘भगवान श्रीस्वामिनारायण’ ही होता है। क्योंकि अन्ततोगत्वा धर्म पिता के पुत्र-पौत्रों ने भी भगवान श्रीस्वामिनारायण का ही आश्रय ग्रहण किया था। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ३. सत् शब्द से वर्णित भगवान, सत्पुरुष, सद्धर्म और सच्छास्त्र, इन चारों का यथायोग्य संग। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ४. साधुरूप तीर्थक्षेत्र |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ५. यहाँ राधिका के सहित श्रीकृष्ण भगवान के ध्यान का आदेश दिया गया है। इस दृष्टांत से श्रीहरि के उत्तम भक्त अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी तथा ब्रह्मस्वरूप सत्पुरुष के साथ भगवान स्वामिनारायण का ध्यान करना चाहिए ऐसा तात्पर्यार्थ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ६. सत्-असत् के ज्ञान से संपन्न। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ७. आत्मा, परमात्मा आदि स्वरूप के ज्ञानयुक्त। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 8 | ८. चिद्रूप, स्वयंप्रकाश तथा अछेद्य, अभेद्य स्वरूप आदि। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 9 | ९. ज्ञानसत्तामात्र। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 10 | १०. अक्षरधाम में मूर्तिमान सेवकरूप में तथा ब्रह्मधाम के रूप में। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | ११. ‘गोलोक में ब्रह्मज्योति’ का अर्थ अनंत गोलोकों के बीच अक्षरधाम सर्वोच्च है। जैसे कि अन्य पर्वतों के बीच हिमालय सबसे बड़ा है, उस प्रकार ‘गोलोक में ब्रह्मज्योति’ कि विभावना है, परंतु ‘गोलोक के भीतर अक्षरधाम अर्थात् ब्रह्मज्योति का समावेश है’ यह आशय नहीं है। (वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण - ६३) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | १२. स्वरूप-स्वभाव से अत्यन्त विलक्षण। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 13 | १३. तीन कालों में भी जिसके स्वरूप का लोप नहीं होता। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 14 | १४. माया और उसके कार्य को जाननेवाले। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | १५. स्वयं जड है, तथा प्रलयकाल में जीव एवं ईश्वररूप चैतन्य को अपने गर्भ में समाविष्ट करनेवाली चित् है, इस प्रकार जड-चिदात्मक। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 16 | १६. कारण अवस्था में पृथ्वी आदि विशेष तत्त्वों से रहित। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 17 | १७. सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की समता रखनेवाली। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 18 | १८. जिसमें रजोगुण, तमोगुण के स्पर्श से रहित शुद्धसत्त्वगुण की प्रधानता रहती है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 19 | १९. मात्रा अर्थात असाधारण गुण। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 20 | २०. ‘प्रधानपुरुष’ शब्द से बहुवचन समझना। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | २१. विराट का दिन पूर्ण होता है उस निमित्त को लेकर ‘निमित्त’ शब्द कहा गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 22 | २२. वैराजपुरुष की आयुष्य के प्रथम अर्ध भाग को परार्ध कहा जाता है। उस परार्ध का प्रथम दिन अर्थात् प्रथम कल्प को ब्राह्मकल्प कहते हैं। (श्रीमद्भागवत: ३/११/३३-३४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 23 | २३. उपरोक्त प्रथम कल्प के अंतिम दिन को पाद्मकल्प कहते हैं। (श्रीमद्भागवत: ३/११/३५) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 24 | २४. हिरण्यकेशीयशाखाश्रुतिः, यह शाखा वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 25 | २५. भावार्थ: अनेक जन्म के पुण्यकर्म द्वारा सिद्ध स्थिति प्राप्त होने पर उसे अंतिम जन्मरूप परागति प्राप्त होती है अर्थात् प्रकट भगवान की प्राप्ति होती है। (गीता: ६/४५) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 17 | 26 | २६. गृहस्थ एवं त्यागियों के लिए श्रीहरि ने शिक्षापत्री आदि ग्रंथों में कहे गए भक्तपोषक सदाचाररूप नियम धर्म। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 18 | 27 | २७. छः दर्शन: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, वेदांत। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 18 | 28 | २८. अठारह पुराण: ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, अग्नि, नारदीय, मार्कंडेय, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड, ब्रह्मांड। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21 | 29 | २९. भगवान के धाम की ओर जानेवाले मार्ग को अर्चिमार्ग, देवयान तथा ब्रह्मपथ भी कहते हैं। उस मार्ग में प्रथम अर्चि (ज्योति) आने के कारण उसे अर्चिमार्ग कहते हैं। [ब्रह्मसूत्र (४/३/१), छांदोग्योपनिषद् (५/१०/१-२), गीता (८/२४)] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 21 | 30 | ३०. साकार एवं निराकार। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 21 | 31 | ३१. अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्यापक चिदाकाश एवं साकार होने पर भी अत्यंत विशालता के कारण निराकार सदृश धाम। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 21 | 32 | ३२. दिव्य करचरणादिक अवयवों से युक्त सेवकरूप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 | 33 | ३३. स्थानरूप अक्षर। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 21 | 34 | ३४. सेवकरूप अक्षर का साधर्म्य। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 21 | 35 | ३५. साधर्म्य अर्थात् समान गुणों से युक्त। जिस प्रकार अक्षरब्रह्म अत्यंत स्नेहपूर्वक परब्रह्म की निरंतर सेवा करने की योग्यता से संपन्न है, उस प्रकार अक्षररूप मुक्त भी ऐसी ही योग्यता प्राप्त करता है; यह अक्षरब्रह्म का साधर्म्य कहा जाता है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 | 36 | ३६. आत्मा-परमात्मा के साक्षात् यथार्थ अनुभव-रूप ज्ञान तथा भगवान के स्वरूप में मन की स्थिरतारूप स्थिति। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 | 37 | ३७. गणपति तथा विष्णु आदि के स्थान सम्बंधी जानकारी: आधार आदि छः चक्र तथा सातवें ब्रह्मरंध्र का वर्णन, योगशिखोपनिषद् के संदर्भानुसार (१/१६८-१७५) दिया गया है।
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 | 38 | ३८. राधा, लक्ष्मी आदि भगवान के स्त्री भक्तों के स्वरूप का वर्णन करनेवाले कीर्तन रसिक कीर्तन हैं। ऐसे कीर्तन गानेवाले का लक्ष्य बदल जाने से उसे कल्याण मार्ग से पतन होने का दोष लग जाता है, यही भावार्थ समझना। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 29 | 39 | ३९. पूर्वसंस्कार अर्थात् अगले जन्मों में संचित एवं इस शरीर की उत्पत्ति में कारणरूप प्रारब्ध कर्म। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 29 | 40 | ४०. भगवान को प्रारब्ध कर्म का सम्बंध न होने पर भी उन्होंने मनुष्यरूप धारण किया है, इसलिए यहाँ ‘प्रारब्ध’ शब्द से श्रीहरि अपनी बात करते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | 41 | ४१. मायिक विषयभोग को जुटाने के संकल्प। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | 42 | ४२. वासना की तीव्रता का असर। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | 43 | ४३. पुनः संकल्प का उत्थान ही न हो ऐसी स्थिति। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 31 | 44 | ४४. अपनी वाणी, क्रिया आदि से किसी को भी दुःख न पहुँचे उस प्रकार एकांत में अंतर्वृत्ति करके रहना। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 32 | 45 | ४५. माया से परे केवल दो ही अनादि तत्त्व हैं: ब्रह्म एवं परब्रह्म। अतः यहाँ नारद-सनकादिक के लिए प्रयुक्त ‘अनादि मुक्त’ शब्द प्रसिद्धि परक समझना चाहिए। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 33 | 46 | ४६. अति दृढ़ विश्वासपूर्वक। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 33 | 47 | ४७. व्रजवासियों की भाँति। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 33 | 48 | ४८. नारद-सनकादि की तरह। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 33 | 49 | ४९. सगुणभाव अर्थात् ज्ञान, आनंद आदि गुण. निर्गुण भाव अर्थात् मायिक गुणों से रहित होने का भाव। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 33 | 50 | ५०. स्वरूप, स्वभाव, गुण, विभूति एवं अवतारों से श्रेष्ठ। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 33 | 51 | ५१. शुष्कवेदान्ती आदि लोगों के द्वारा। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 35 | 52 | ५२. भगवान अथवा भगवान के भक्त के अवगुण ग्रहण करने के कारण। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 37 | 53 | ५३. सांसारिक दृष्टि से मंदबुद्धि एवं गरीब स्वभाववाला। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 37 | 54 | ५४. यमराज आदि का। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 37 | 55 | ५५. अक्षरब्रह्ममय दिव्य शरीर से युक्त। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 38 | 56 | ५६. एक व्यक्ति को भूत अपने वश में आ गया। वह उसका हर एक काम पल भर में निपटा लेता और जैसे ही फुर्सत पाता, उस व्यक्ति को कहता कि, “अब मैं तुझे खा जाऊँगा।” उसने परेशान होकर एक महात्मा को अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि, “जब तुम्हें भूत का कोई काम हो, तो बुला लेना और खाली समय में उसको एक खंभे के ऊपर लगातार चढ़ने-उतरने के लिए भेज देना।” इस प्रकार करने से भूत को कभी फुर्सत ही नहीं मिली और उसने कभी अपने मालिक को परेशान भी नहीं किया। इस प्रकार मन को हमेशा भगवान के लीलाचरित्रों में प्रवृत्त रखना चाहिए; अन्यथा वह फुर्सत पाते ही व्यक्ति को खा जाता है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 38 | 57 | ५७. रुचिकर वस्तुओं का लाभ नहीं होता, परंतु उसके बदले में अरुचिकर वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 38 | 58 | ५८. महाभारत, शांतिपर्व: ३१६/४०, ३१८/४४; यहाँ धर्मादि का स्वरूपतः त्याग नहीं कहा गया किन्तु भगवान के ध्यान में विघ्न करने वाले संकल्पों का त्याग कहा गया है अथवा एसे ही फल का त्याग कहा गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 38 | 59 | ५९. मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदि का ज्ञाता, निश्चयकर्ता, दृष्टा, श्रोता, वक्ता, स्वाद लेनेवाला आदि क्रियाओं में जो लिप्त है वही जीवात्मा है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 39 | 60 | ६०. परब्रह्म को निराकार एवं निर्गुण प्रतिपादन करनेवाले शुष्कज्ञानी सीप में जैसे कोई चांदी को देखता है, परंतु सीप में चांदी तो नहीं है, उसी प्रकार उपरोक्त तत्त्व भी नहीं है, इस प्रकार तत्त्वों को मिथ्या दिखाते है, यही भावार्थ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 40 | 61 | ६१. योगदर्शन में इन दोनों प्रकार की समाधियों का वर्णन कठिनरूप से किया गया है। (योगसूत्र: १/१७,१८, ध्यानदीप: १२६-१२९) परंतु भगवान स्वामिनारायण ने दोनों समाधियों को अत्यंत सरल ढंग से निरूपित किया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सविकल्प समाधि में उपास्य एवं उपासक दोनों की शुद्धि नहीं है, जबकि निर्वकल्प समाधि में उपासक गुणातीत है, अर्थात् अक्षरब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त हुआ है तथा उपास्य इष्टदेव मायिक गुणों से परे परमात्मा है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 40 | 62 | ६२. भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तनों का गान, स्मृति, चरण-सेवा, अर्चन-पूजा, अष्टांग अथवा पंचांग प्रणाम, दासभाव पूर्वक आज्ञापालन, निष्कपटभाव, सर्वस्व सर्मपण - ये नव प्रकार की भक्ति कही गई है। (श्रीमद्भागवत: ७/५/२३) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 41 | 63 | ६३. ‘तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय’ इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद् (६/२/३) में पाठान्तर प्राप्य है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 41 | 64 | ६४. श्रीमद्भागवत: १०/८७/१९ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 41 | 65 | ६५. सर्वव्यापक पुरुषोत्तम भगवान का प्रवेश सर्वदा, सर्व वस्तुओं में अनादि काल से है; इसलिए यहाँ जिसे ‘प्रवेश’ कहा गया है, वह विशिष्ट शक्तियों से युक्त अनुप्रवेश समझना। (तैत्तिरीयोपनिषद्: २/६) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 41 | 66 | ६६. अब प्रारंभ होनेवाले वाक्यों का अर्थ यह है कि परब्रह्म स्वयं, अक्षरब्रह्म के द्वारा जैसा सामर्थ्य दिखाते हैं, वैसा सामर्थ्य प्रकृतिपुरुष आदि द्वारा दिखाते नहीं हैं। इसमें पात्रता का भेद कारणभूत है। जैसे सूर्य की किरणें मिट्टी पर इतनी परावर्तित नहीं होतीं, जितनी पानी अथवा काँच पर परावर्तित होती हैं। यहाँ सूर्य की किरणें कारणभूत नहीं है, किन्तु पात्रों की पात्रता का भेद कारणभूत है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 41 | 67 | ६७. ‘सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।’ (गीता ११/४०) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 42 | 68 | ६८. ‘चर्पटपंजरीका स्तोत्र,’ ‘यतिधर्मनिर्णय,’ ‘संन्यासधर्मपद्धति,’ ‘साधनपंचकम्’ - आदि शंकराचार्य रचित ग्रंथों में विधि-निषेध के आदेश प्राप्त होते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 43 | 69 | ६९. मेरी सेवा से प्राप्त होनेवाली सालोक्यादि चतुर्विध मुक्ति को मेरी सेवा से ही परिपूर्ण हुए निष्काम भक्त नहीं चाहते, तब वे फिर काल द्वारा नष्ट होनेवाले देवताओं के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की इच्छा न करें, उसके सम्बंध में क्या कहना? (श्रीमद्भागवत: ९/४/६७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 43 | 70 | ७०. अर्थ: मेरी सेवा के सिवा भगवान द्वारा बलपूर्वक प्रदत्त सालोक्यादि मुक्ति को भी जब निर्गुण भक्तिवाले ग्रहण नहीं करते, तब फिर वे सांसारिक फल की इच्छा न करें, उसके सम्बंध में क्या कहना? (श्रीमद्भागवत: ३/२९/१३) आत्यंतिक मुक्ति में चार भेद नहीं है। भगवान स्वामिनारायण ने आत्यंतिक मुक्ति का लक्षण इस प्रकार कहा है: तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवामुक्तिश्च गम्यताम्। (शिक्षापत्री १२१) अर्थात् “अक्षरधाम को प्राप्त अक्षरमुक्त अक्षरब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त होता है।” (वचनामृत गढ़डा प्रथम २१) इस प्रकार उन्होंने ‘ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा’ को ही मुक्ति के रूप में स्वीकार किया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 43 | 71 | ७१. अर्थ: अर्चिरादिमार्ग में जाना आरम्भ होने के बाद मेरे निष्काम भक्त मेरी - योगमाया के स्वामी की प्रसिद्ध विभूति को, ब्रह्मलोक तक की सम्पत्ति, भक्तियोग से प्राप्त होनेवाले अणिमादि आठ प्रकार के ऐश्वर्यों को तथा वैकुंठादि दिव्य-लोकों में रहनेवाली सम्पत्ति को, अर्थात् मंगलरूप भागवती श्री को प्राप्त करना नहीं चाहते। फिर भी सबसे परे मेरे धाम में जाकर वे उन्हें प्राप्त करते हैं। यदि मेरे ये भक्त ‘भागवती श्री’ तक को नहीं चाहते हैं, तो वे माया-विभूति आदि की इच्छा न करें, इसमें कहना ही क्या है? (श्रीमद्भागवत: ३/२५/३७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 45 | 72 | ७२. ‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। (श्वेताश्वतरोपनिषद्: ३/१९) इत्यादि श्रुतियों से। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 45 | 73 | ७३. ‘य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुर्हिरण्यकेश... तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकमेवमक्षिणी।’ (छान्दोग्योपनिषद्: १/६/६-७) इत्यादि श्रुतियों से। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 45 | 74 | ७४. ‘स ईक्षत’ (ऐतरेयोपनिषद्: ३/१) इत्यादि श्रुतियों से। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 45 | 75 | ७५. यहाँ अपने तेज को ‘ब्रह्म’ कहा गया है, परन्तु ‘धामरूप अथवा सेवकरूप अक्षरब्रह्म’ नहीं समझना चाहिए। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 46 | 76 | ७६. आकाश के दो प्रकार हैं: भौतिक तथा महाकाश। योगी महाकाश को ही चिदाकाश कहते हैं। समाधि में चिदाकाश का लय नहीं होता परंतु भौतिक आकाश का संकोचनरूप लय होता है, यही भावार्थ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 49 | 77 | ७७. षट्चक्र की विशेष जानकारी के लिए देखिए: वचनामृत गढ़डा प्रथम २५ की पादटीप क्रमांक: ३७ गणपति तथा विष्णु आदि के स्थान सम्बंधी जानकारी: आधार आदि छः चक्र तथा सातवें ब्रह्मरंध्र का वर्णन, योगशिखोपनिषद् के संदर्भानुसार (१/१६८-१७५) दिया गया है।
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 50 | 78 | ७८. गीता: २/६९ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 52 | 79 | ७९. मोक्षधर्म की। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 54 | 80 | ८०. श्रीमद्भागवत: ३/२५/२० |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 56 | 81 | ८१. गीता: ७/१६-१७; ज्ञानी स्वयं को ब्रह्मरूप मानकर एकमात्र परमात्म-भक्ति की ही अभिलाषा रखता है, इसी कारण आर्त, जिज्ञासु तथा अर्थार्थी से अधिक कहा गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 57 | 82 | ८२. अर्थात् भगवान के मनुष्य-चरित्रों को देखते हुए भी क्षीण न होनेवाला, सुदृढ़ एवं प्रतिदिन बढ़नेवाला स्नेह, जो मूढ़तापूर्ण स्नेह से अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 59 | 83 | ८३. जाम्बवान ने हनुमानजी को उनके बल का बोध कराया था, उसे वाल्मीकि रामायण में ‘जाम्बवान् समुदीक्ष्यैवं’ इत्यादि वचनों से कहा गया है। (किष्किन्धाकांड, सर्ग: ६५) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 59 | 84 | ८४. श्रीकृष्ण भगवान ने बलदेवजी को उनके बल से अवगत कराया था, उसे विष्णुपुराण में ‘इति संस्मारितो विप्र’ इत्यादि वचनों से कहा गया है। (विष्णुपुराण: ५/९/३४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 61 | 85 | ८५. आत्मनिष्ठा से युक्त उपासना। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 62 | 86 | ८६. १. सत्यम् - सर्वभूतप्राणिमात्र का हित करना अथवा सत्य वचन बोलना। २. शौचम् - समस्त हेय का विरोधी भाव अर्थात् निर्दोष भावना। ३. दया - दूसरे के दुःख को सहन न करना। ४. क्षान्तिः - अपराधी पुरुष के अपराध को सहन करना। ५. त्यागः - याचकों के प्रति उदारता अथवा आत्मसमर्पण। ६. सन्तोषः - सदा क्लेशरहित रहने का भाव। ७. आर्जवम् - मन, वाणी तथा कर्म की एकरूपता। ८. शमः - मन का निग्रह करना। ९. दमः - बाह्य इन्द्रियों का निग्रह करना। १०. तपः - शरीर एवं मन को क्लेश हो, ऐसे व्रतादि को करना। ११. साम्यम् - शत्रु-मित्रादि के प्रति समान भावना से रहना। १२. तितिक्षा - सुखदुःखादि के द्वन्द्वों से परास्त नहीं होना। १३. उपरतिः - अधिक लाभ एवं प्राप्ति के प्रति उदास रहना। १४. श्रुतम् - समस्त शास्त्रों के अर्थों का यथार्थ ज्ञान होने का भाव। १५. ज्ञानम् - आश्रितों के अनिष्ट की निवृत्ति तथा इष्ट की प्राप्ति कराने में उपयोगी ज्ञान। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म तथा परब्रह्म की अनुभवपूर्ण जानकारी। १६. विरक्तिः - विषयों में निःस्पृहभाव अथवा विषयों से चित्त का अनाकर्षण। १७. ऐश्वर्यम् - सबका नियन्ता होने का भाव। १८. शौर्यम् - शूरवीरता। १९. तेजः - किसी से भी पराजित न होने का भाव। २०. बलम् - सबकी प्राणवृत्तियों का नियमन करने का सामर्थ्य। २१. स्मृतिः - भक्तों के अपराधों को भूलकर, उनके गुणों का स्मरण करना। २२. स्वातन्त्र्यम् - दूसरे की अपेक्षा से रहित रहने की भावना। २३. कौशलम् - निपुणता। २४. कान्तिः - आध्यात्मिक तेज़। २५. धैर्यम् - सर्वदा अव्याकुलता। २६. मार्दवम् - चित्त की कोमलता। क्रूरता से रहित रहने का भाव। २७. प्रागल्भ्यम् - ज्ञान की गंभीरता, प्रगल्भता। २८. प्रश्रयः - विनयभाव तथा ज्ञानपूर्वक आत्मसात् हुआ दीनभाव। २९. शीलम् - सत्याचरण। ३०. सहः - प्राणों को नियमन करने का सामर्थ्य। ३१. ओजः - ब्रह्मचर्य से प्राप्त की गई दिव्य कांति। ३२. बलम् - कल्याणकारी गुणों को धारण करने का सामर्थ्य। ३३. भगः - ज्ञानादि गुणों का उत्कर्ष। ३४. गाम्भीर्यम् - ज्ञान की गहनता, छिछोरापन से रहित होने का भाव। अथवा अभिप्राय ज्ञात न हो सके, ऐसा आंतरिक गुण। ३५. स्थैर्यम् - क्रोध का निमित्त होने पर भी विकार न होना। अचंचलता। ३६. आस्तिक्यम् - शास्त्रों के अर्थों में विश्वास। भगवान सदा कर्ता, साकार, सर्वोपरि एवं प्रगट हैं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा। ३७. कीर्तिः - यश। ३८. मानः - पूजा-सम्मान की योग्यता। ३९. अनहंकृतिः - अहंकार का अभाव। निर्मानीता। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 62 | 87 | ८७. कुटिल युक्तिजाल से मन को संशयग्रस्त करनेवाले असच्छास्त्र। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 64 | 88 | ८८. ‘यस्यात्मा शरीरम्’ (बृहदारण्यकोपनिषद्: ३/७/३०) आदि। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 64 | 89 | ८९. ‘शीर्यते तच्छरीरम्’, जो विशीर्ण होता है, उसे शरीर कहा जाता है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति से शरीर का जो शब्दार्थ है, वह निर्विकारी आत्मा तथा अक्षर के सम्बंध में किस तरह सम्भव होता है, यही प्रश्नार्थ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 64 | 90 | ९०. ‘शीर्यते तच्छरीरम्’, यहाँ उपरोक्त अर्थ नहीं बताया गया। परंतु उपनिषद् में उल्लिखित शरीर शब्द का पारिभाषिक अर्थ व्याप्यता, अधीनता तथा असमर्थता किया गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 64 | 91 | ९१. कर-चरणादिक अवयवरहित होने के कारण अरूप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 64 | 92 | ९२. ऐश्वर्य अर्थात् माया के गुणों से पराभूत न होने का सामर्थ्य। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 64 | 93 | ९३. सुषुप्ति तुल्य अक्षरब्रह्मतेज में। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 64 | 94 | ९४. यदि वह कोई ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं करता, तो भगवत् सेवा का आनंद तो मिलेगा ही कैसे? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 65 | 95 | ९५. नित्य तत्त्व में तीन भेद हैं: (१) कूटस्थ नित्य: तीनों काल में परिणामगामी नहीं होता है उसे कूटस्थ नित्य कहा जाता है। (२) प्रवाह नित्य: गाँव या शहर में सैकड़ों सालों में प्रजा परिवर्तित होती रहती है। परंतु गाँव या शहर की उम्र सैकड़ों सालों की ही कही जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मांडों की महाउत्पत्ति के समय पुरुष बदल जाने पर भी उसी के नाम से विद्यमान स्थान तथा उत्पत्ति में कारणभूत स्थान को नित्य कहा जाता है। (३) परिणामी नित्य: परिणाम बदलते रहने पर भी तत्त्व नहीं बदलता है। जैसे स्वर्ण वही रहने पर भी उसके विविध गहने बनते हैं। उसी प्रकार माया की परिणाम गामी नित्यता समझना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में प्रकृति पुरुष की तरह आकाश की नित्यता कही है। परंतु पुरुष, प्रकृति एवं चिदाकाश तीनों तत्त्वों की नित्यता में अंतर है। इस प्रकार चिदाकाश कूटस्थ नित्य है, एवं प्रकृति परिणामगामी नित्य है तथा पुरुष प्रवाह नित्य है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 65 | 96 | ९६. भगवान सभी जीवों के गुणकर्मानुसार जीव में ज्ञान आदि शक्तियों को प्रेरित करते हैं। अतः भगवान में कोई विषमता नहीं है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 66 | 97 | ९७. शाब्दिक व्याख्याएँ; निरूपण |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 66 | 98 | ९८. यहाँ ब्रह्म शब्द से भूमापुरुष का लोक समझना चाहिए। - भागवत: १०/८९/५३-५८ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 68 | 99 | ९९. ‘शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती। मणिमयी मनोमयी प्रतिमाष्टविधाः स्मृताः॥’ (श्रीमद्भागवत: ११/२७/१२) पत्थर, काष्ट, धातु, चित्रप्रतिमा, रेखाकृति, रेत, मणिमयी और मानसिकी - इस प्रकार मूर्तियों के आठ भेद हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 70 | 100 | १००. गीता: १८/७८ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 71 | 101 | १०१. यहाँ निर्देशित अक्षरधाम अर्थात् भगवान स्वामिनारायण के साथ पृथ्वी पर पधारे हुए संत सद्गुरुवर्य गुणातीतानंद स्वामी थे। जिनकी पहचान स्वयं श्रीहरि ने बारबार करवाई थी। इसी कारण वे संप्रदाय में अपने ही समय में ‘अक्षरब्रह्म’ एवं ‘वचनामृत-रहस्य के ज्ञाता’ के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 71 | 102 | १०२. इस पृथ्वी पर अक्षर सहित पुरुषोत्तम अर्थात् गुणातीतानंद स्वामी के साथ श्रीहरि सर्वदा प्रकट रहते हैं। इसी ज्ञान को ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज ने इन दोनों की मूर्तियों की स्थापना करके मूर्तिमान बनाया। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 73 | 103 | १०३. जल में नाभि तक खड़े रहकर गुदा द्वारा जल को खिंचकर और बस्ति (नाभि से निचले भाग) को धोकर उसे निकाल डालना चाहिए, अर्थात् गुदामार्ग से चढ़ाये गए जल को गुदा द्वारा ही बाहर निकाल देना, उसे बस्तिक्रिया का एक प्रकार कहा जाता है। लिंग द्वारा पानी को चढ़ाने के बाद उसे फिर से लिंग द्वारा ही अथवा गुदामार्ग से बाहर निकाल देना, इसे बस्तिक्रिया का दूसरा प्रकार कहा गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 73 | 104 | १०४. सर्व प्रथम मुख से जल पीकर उसका फिर से मुँह के जरिये ही वमन कर डालना, उसे गजकरणी क्रिया कहा जाता है और उसको कुंजरक्रिया भी कहते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 73 | 105 | १०५. भद्रासन को ही गोरक्षासन कहते हैं। वृषण (अंडकोश) के नीचे के लिंगसूत्र के दोनों पार्श्वभागों में गुल्फा को रखना चाहिए, उसमें वाम गुल्फा को लिंग के नीचे के सूत्र के बाँये भाग में और दक्षिण गुल्फा को उस सूत्र के दक्षिण भाग में रखना चाहिए तथा सूत्र के पार्श्वभाग के समीप रखे हुए दोनों पैरों को दोनों हाथों से, जो पश्चिम की ओर लोम-विलोम किए हुए रहें, ग्रहण करना चाहिए। इस क्रिया को उत्तम भद्रासन कहा गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 75 | 106 | १०६. एकोत्तर शब्द से एकोत्तरशत (१०१) अथवा एकोत्तरविंशति (२१) कहने का अभिप्राय है। दस पूर्व के और दस बाद के कुलों तथा स्वयं के एक कुल को मिलाकर इक्कीस कुलों का उद्धार हो जाता है, ऐसा श्रीमद्भागवत में (७/१०/१८) भगवान नृसिंह ने कहा है। यह भी कहा गया है कि पिता के २४, माता के २०, भार्या के १६, भगिनी के १२, दुहिता के ११, बुआ के १०, मौसी के ८, इस प्रकार सात गोत्रों को मिलाकर १०१ कुलों का उद्धार हो जाता है। उल्लिखित माता-पिता आदि के कुलों में आधे पूर्व के और आधे बाद के समझने चाहिए। (निर्णयसिंधु: ३/२, पृ. २६७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 77 | 107 | १०७. कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्। १. कृपालुः - स्वार्थ की अपेक्षा किए बिना ही दूसरे का दुःख सहन न हो, ऐसा पुरुष, अथवा दूसरे के दुःख को टालने की इच्छावाला। २. सर्वदेहिनाम् कृतद्रोहः - समस्त प्राणियों में मित्रादि भाव रखनेवाला और किसी का भी द्रोह न करनेवाला। ३. तितिक्षुः - द्वन्द्व को सहन करनेवाला। ४. सत्यसारः - सत्य को ही एक मात्र बल माननेवाला। ५. अनवद्यात्मा - द्वेष, असूया आदि दोषों से रहित मनवाला। ६. समः - सभी में समदृष्टिवाला। ७. सर्वोपकारकः - सबका उपकार ही करनेवाला। ८. कामैरहतधी: - विषयभोग से बुद्धि में क्षोभ -प्राप्त नहीं करनेवाला। ९. दान्तः - इन्द्रियों का दमन करनेवाला। १०. मृदुः - मृदुचित्तवाला। ११. शुचिः - बाह्य एवं आन्तरिक रूप से पवित्रता रखनेवाला। स्नानादिजन्य शुचिता को बाह्य पवित्रता तथा भगवान के चिन्तन से उत्पन्न शुचिता को आन्तरिक पवित्रता कहा गया है। १२. अकिंचनः - अन्य प्रयोजनों से रहित। १३. अनीहः - लौकिक व्यापाररहित अथवा किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित। १४. मितभुक् - मिताहार करनेवाला। १५. शान्तः - जिसका अन्तःकरण नियमानुवर्ती है। १६. स्थिरः - स्थिरचित्तवाला। १७. मच्छरणः - जिसका मैं ही रक्षक और प्राप्ति का उपाय हूँ। १८. मुनिः - शुभाशय का मनन करनेवाला। १९. अप्रमत्तः - सावधान। २०. गभीरात्मा - जिसका अभिप्राय न जाना जा सके, ऐसा पुरुष। २१. धृतिमान् - धैर्य रखनेवाला। २२. जितषड्गुणः - अशन, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु इन छः द्वन्द्वों पर विजय प्राप्त करनेवाला। २३. अमानी - अपने सत्कार की अभिलाषा नहीं रखनेवाला। २४. मानदः - दूसरों का सम्मान करनेवाला। २५. कल्पः - हितकारी उपदेश करने में समर्थ। २६. मैत्रः - किसी को भी नहीं ठगनेवाला। २७. कारुणिकः - निःस्वार्थ, अलोभ रहकर केवल करुणापूर्ण व्यवहार करनेवाला। २८. कविः - जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म - इन पाँच तत्त्वों को यथार्थ जाननेवाला। २९. “वेद द्वारा प्रतिपादित गुणदोषों को जानकर तथा अपने समस्त धर्मों को फल द्वारा त्याग करके, जो उपायोपेयभाव से मेरा भजन करता है,” उसे उत्तम साधु जानना चाहिए। ३०. “मैं जैसा स्वरूपवाला हूँ और जितनी विभूतियों से सम्पन्न हूँ, उन्हें जानकर, यानि उन पर बार-बार विचार करके अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसे ही उत्तम भक्त माना गया है।” इस प्रकार साधु के तीस लक्षण कहे गए हैं। (श्रीमद्भागवत: ११/११/२९-३३) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 77 | 108 | १०८. भावार्थ: उसके दो कारण हैं: काल और अवस्था। ये दोनों ही शुभ अथवा अशुभ होते हैं। यदि अन्त समय में ये दोनों शुभ रहे तो मृत्यु तेजोमय होती है, परंतु अशुभ बने रहे तो मरणकाल कष्टदायक होता है। मरणोत्तर गति में तो शुभाशुभकाल या अवस्था कारणभूत नहीं होते। उसमें तो अपना धर्माचरण ही कारण बनता है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 79 | 109 | १०९. मणिरत्नमाला: ११ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 81 | 110 | ११०. ‘दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि। ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम्।’ (श्रीमद्भागवत: ३/२/८) इस श्लोक का यही भावार्थ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 84 | 111 | १११. स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण नामक तीन देहों के अभिमान से जीव का विश्व, तेजस् और प्राज्ञ नाम से तीन नामाभिधान हुआ है। जो कि वास्तविक नहीं, किन्तु उपाधि के कारण है। इसीलिए यहाँ ‘विश्वाभिमानी’ शब्द का प्रयोग किया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 84 | 112 | ११२. जीव विषयों को जानता है, वही ज्ञातृत्व है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 84 | 113 | ११३. जीव अहंवृत्ति के कारण विषयों के लिए कर्म करता है, वही कर्तृत्व है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 84 | 114 | ११४. सगुणब्रह्मरूप प्रधानपुरुष। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 84 | 115 | ११५. कर्म करनेवाला जो जीव है, इस प्रकार की वृत्ति की। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 84 | 116 | ११६. रजोगुणप्रधान। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 84 | 117 | ११७. यहाँ ब्रह्म और परब्रह्म दोनों को अलग तत्त्व के रूप में निर्देशित किया गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 87 | 118 | ११८. ‘स्थान’ का अर्थ यहाँ कोई मठ, मंदिर अथवा सम्प्रदाय तक सीमित नहीं है, परंतु धर्मनिष्ठा ही श्रीहरि के मतानुसार सच्चा ‘स्थान’ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 88 | 119 | ११९. अंतर्दृष्टिवालों की तुलना में बाह्यदृष्टिवालों की स्थिति तथा समझ अल्प गुणकारी है, ऐसा मिथ्या शब्द का अर्थ समझना चाहिए। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 89 | 120 | १२०. मुण्डकोपनिषद्: ३/१/३ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 89 | 121 | १२१. गीता: ६/४५ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 92 | 122 | १२२. गीता: १५/६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 93 | 123 | १२३. श्रीमद्भागवत: १०/४७/२७-२८ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 94 | 124 | १२४. श्रीमद्भागवत: १०/८७/६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 95 | 125 | १२५. अनल पक्षी तथा गरुड़ के दृष्टांत से कहे गए इस विधान के द्वारा श्रीहरि ने प्रकृतिपुरुष एवं अक्षरमुक्त में स्थितिभेद का वर्णन किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वचनामृत गढ़डा मध्य १२ तथा वचनामृत गढ़डा मध्य ३१ में प्रकृति के साथ संलग्न होनेवाले पुरुष को ही अक्षरमुक्त कहा गया है - इन परस्पर विरोधी विधानों का समाधान इस प्रकार है कि प्रकृति के साथ संलग्न होनेवाले पुरुष तो प्रवृत्ति-परक है, तथा अन्य अक्षरमुक्त निवृत्ति परक है। दोनों में इतना भेद कहा जाएगा, परंतु दोनों की प्राप्ति तथा स्थिति में कोई अंतर नहीं है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 95 | 126 | १२६. यहाँ मुक्तों के भेद दिखाए गये हैं, वह अक्षरमुक्तों के भेद नहीं है। अक्षरधाम स्थित तमाम अक्षरमुक्त तो ब्रह्म का साधर्म्य प्राप्त करके समान रूप से भगवान के दिव्य आनंद का उपभोग किया करते हैं। परंतु यहाँ उपासना में भेद होने के वैकुंठ आदि धामों को प्राप्त हुए हैं, उनके ये भेद हैं। अर्थात् जिसने भगवान स्वामिनारायण को जिस अवतार के समान समझा, उसे उस अवतार के धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मुक्तों में भेद हो गये। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 97 | 127 | १२७. एक ही समय में एक साथ ही। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 97 | 128 | १२८. यहाँ जीवात्मा को ज्ञानशक्ति के द्वारा इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण आदि पूरे शरीर में व्यापक कहा गया है। परंतु वास्तव में तो वह अणुतुल्य सूक्ष्म है। अद्वैती लोग उसे आकाश की तरह व्यापक मानते हैं, उस मान्यता का श्रीहरि अस्वीकार करते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 97 | 129 | १२९. श्रीमद्भागवत: ५/६/७-८ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 97 | 130 | १३०. तामसकर्म के फलरूप भोग को भुगतने के लिए शक्तिमान करते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 97 | 131 | १३१. राजसकर्म के फलरूप स्वप्न भोग को भुगतने के लिए शक्तिमान करते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 97 | 132 | १३२. सात्त्विककर्म के फलरूप भोग को भुगतने के लिए शक्तिमान करते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 97 | 133 | १३३. जाग्रत और स्वप्न में देह-इन्द्रिय आदि भावों से सहित। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 97 | 134 | १३४. सुषुप्ति में देह-इन्द्रिय आदि भावों रहित। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 97 | 135 | १३५. अपने-अपने कार्य के लिए शक्तिमान करते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 97 | 136 | १३६. श्रीमद्भागवत: १०/८७/२ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 97 | 137 | १३७. मुंडक उपनिषद्: ३/१/३; गीता: ४/१० |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 97 | 138 | १३८. कैवल्यार्थी अर्थात् आत्मा को ही परमात्मा माननेवाला; भक्तिरहित। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 98 | 139 | १३९. जैन दर्शन में जीव, अजीव आदि सात तत्त्वों का स्वीकार किया गया है। इनमें अजीव तत्त्व के अन्तर्गत पुद्गल का समावेश होता है। यह पुद्गल मूर्तिमान है। पुद्गलों की वर्गणा ही कर्मरूप बनकर जीवों को बंधन करती है। इस प्रकार पुद्गल मूर्तिमान होने के कारण कर्म को भी मूर्तिमान कहा है। (तत्त्वसमाससूत्र: १/४; ५/१,४; ८/२) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 100 | 140 | १४०. जीव में अंतर्यामीरूप से रहने वाले परमात्मा का। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 100 | 141 | १४१. जीव अपनी ज्ञातृत्वशक्ति द्वारा संपूर्ण देह एवं बुद्धि में व्याप्त है। बुद्धि मायिक कार्य होने से जड़ होती है। उसमें स्वतः ज्ञातृत्व संभव नहीं है, वह तो जीव को ज्ञातृत्व शक्ति से ही कार्य करने के लिए समर्थ होती है। इसी कारण जीव का ज्ञातृत्व कहनसे ‘बुद्धि का ज्ञातृत्व’ कहा जाता है। उसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा में व्याप्त है, ऐसे साक्षीभाव से रहनेवाले परमात्मा की ही कार्यशक्ति के कारण जीवात्मा जानना, सुनना आदि बौद्धिक क्रिया करने में समर्थ होती है। अतः साक्षीरूप परमात्मा का ज्ञातृत्व कहने से जीवात्मा का ज्ञातृत्व कहा गया है। यही तात्पर्यार्थ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 102 | 142 | १४२. श्रीमद्भागवत: १/१/२ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 104 | 143 | १४३. श्रीजीमहाराज यहाँ ‘सगुण’ और ‘निर्गुण’ इन दोनों शब्दों का ‘गुणसहित’ तथा ‘गुणरहित’ अर्थ से भिन्न निरूपण करते हैं, जिसे कठोपनिषद् (१/२/२०) में ‘अणोरणीयान्’ आदि श्रुतियों में कहा गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 106 | 144 | १४४. यहाँ ‘प्रकृति’ शब्द से प्रधान-प्रकृति समझकर ‘प्रधानपुरुष’ का संदर्भ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 106 | 145 | १४५. यहाँ ‘ब्रह्म’ शब्द से अक्षरब्रह्मात्मक मुक्त अथवा ‘प्रकृतिपुरुष’ का संदर्भ समझना। वचनामृत गढ़डा मध्य ३१ में उन्हीं को ‘ब्रह्म’ कहा गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 110 | 146 | १४६. माया-प्रकृति जड तत्त्व है, जिसे वचनामृत गढ़डा प्रथम १२ में निर्विशेष कही गई है। अतः प्रलयावस्था में वह स्त्री-आकारवाली नहीं हो सकती। परंतु नारी जाति वाचक शब्द होने से, तथा प्रजातुल्य प्रधानपुरुष के कारणरूप होने से उसे ‘स्त्री-आकारवाली’ कहा गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 111 | 147 | १४७. श्रीमद्भागवत: ७/९/१५, ७/१०/७-८ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 112 | 148 | १४८. प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यह है कि, “अन्य ब्रह्मांडों में भगवान मनुष्याकार में प्रकट होते हैं या नहीं?” श्रीहरि अभिप्राय देते हैं कि अपने अनन्य भक्तों को दर्शनादिक का आनंद देने के लिए भगवान कृपा करके स्वेच्छापूर्वक अन्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 112 | 149 | १४९. श्रीमद्भागवत: ४/२०/३२, ४/७/४४, ९/२१/१७. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 112 | 150 | १५०. झीणाभाई जूनागढ राज्य के सभासद थे, एवं पंचाला गाँव के ठाकुर साहब थे। उनका प्रेमाग्रह था कि श्रीजीमहाराज उनके घर पधारे, परन्तु किसी कारणवशात् श्रीहरि उनके घर नहीं पधारे, झीणाभाई को लगा कि श्रीहरि ने मेरे आमंत्रण का अस्वीकार करके मेरा मानभंग किया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 114 | 151 | १५१. वैष्णव परंपरा के गुजराती भक्तकवि। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 115 | 152 | १५२. अर्थ: “बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती।” (हिरण्यकेशीयशाखा) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 115 | 153 | १५३. अर्थ: “परमात्मा के ज्ञान से ही संसार मृत्यु पर विजय हो सकती है, अतः मुक्ति के लिए ज्ञान के सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है।” (श्वेताश्वतरोपनिषद्: ३/८) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 115 | 154 | १५४. अर्थ: “पूर्वश्लोक में वर्णित स्वभाव से जीवों-ईश्वरों के लिए मैं अतीत हूँ। यानी उनके दोषों का स्पर्श मुझे नहीं होता तथा अक्षरब्रह्म से भी मैं उक्त कारणों से अतिशय उत्कृष्ट हूँ।” (गीता: १५/१८) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 115 | 155 | १५५. अर्थ: “मैं अपने सामर्थ्य के एक अंश से इस जड-चिदात्मक समग्र जगत को धारण किये हुए हूँ।” (गीता: १०/४२) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 115 | 156 | १५६. अर्थ: “हे अर्जुन! मुझसे अतिरिक्त कोई भी तत्त्व परतर नहीं है। जिस प्रकार डोरे में मणिमाला पिरोयी हुई रहती है, उसी प्रकार यह मेरा शरीर भूतचिदचिदात्मक समग्र जगत मुझमें समाया हुआ है, अर्थात् मेरा आश्रित है।” (गीता: ७/७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 115 | 157 | १५७. अर्थ: “हे पार्थ! मेरे अनेक रूपों का तुम अवलोकन करो, जो नाना प्रकार के दिव्य एवं शुक्लादि विभिन्न वर्णवाले तथा नाना आकृतिवाले हैं।” (गीता: ११/५) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 115 | 158 | १५८. अर्थ: “यद्यपि नैष्कर्म्य यानी आत्मा की यथार्थ उपासनारूप ज्ञान निरंजन अर्थात् रागद्वेषादिरूप मायारहित है, फिर भी जो भगवान की भक्ति से रहित है, वह अत्यन्त शोभित नहीं लगता, अर्थात् भक्तियोग से विरत ज्ञानयोग शोभायमान नहीं होता।” (श्रीमद्भागवत: १/५/१२) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 115 | 159 | १५९. अर्थ: “मुमुक्षुओं द्वारा करने योग्य कर्म के सम्बंध में ज्ञान प्राप्त करना है तथा नाना प्रकार के विकर्मात्मक वैदिक काम्यकर्म के विषय में भी जानकारी शेष रही है। इसी प्रकार अकर्मात्मक ज्ञान के सम्बंध में भी ज्ञान प्राप्त करना शेष रहा है। इस रीति से कर्म की गति को गहन माना गया है, अर्थात् उसका स्वरूप ऐसा है कि वह बोधगम्य नहीं हो सकता।” (गीता: ४/१७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 115 | 160 | १६०. अर्थ: “जो ब्रह्मरूप हुआ है, और प्रसन्नमन है, अर्थात् क्लेश-कर्मादि दोषों से जिसका मन कलुषित नहीं हुआ है, और जो किसी पर भी शोक नहीं करता, किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता तथा समस्त प्राणियों में समभाव रखता है, वही मेरी परा भक्ति को प्राप्त करता है।” (गीता: १८/५४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 115 | 161 | १६१. जिनकी भक्ति करने की बात कही गयी है, ऐसे परब्रह्म प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण ही दोनों प्रकृतियों के आधार हैं, यही बात गीता में कही गयी है कि – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 115 | 162 | १६२. अर्थ: “पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन आदि इन्द्रियाँ, महत्तत्त्व तथा अहंकार इस आठ प्रकार की मेरी प्रकृति हैं। अर्थात् मैं अचेतन प्रकृति से विलक्षण हूँ।” (गीता: ७/४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 115 | 163 | १६३. अर्थ: “यह मेरी अपरा (अप्रधानभूता) प्रकृति है, इस अचेतन प्रकृति से विलक्षण आकारवाली परा (प्रधानभूता) एवं चेतनरूप यह प्रकृति मेरी है। ऐसा समझिये कि जो चेतन प्रकृति है, उसने समग्र अचेतन जगत को धारण कर रखा है, अर्थात् मैं चेतन प्रकृति से विलक्षण हूँ।” (गीता: ७/५) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 115 | 164 | १६४. यद्यपि आकाश में संकोच-विकास की अवस्थाएँ वस्तुतः नहीं हैं तथापि वे स्वयं पृथिव्यादि भूतों में व्यापक रूप से रही हैं। उनसे उन भूतों में होनेवाली संकोच-विकास की प्रक्रियाएँ पारस्परिक रूप से आकाश में उपचारमात्र होती हैं। वैसे ही निर्विकारी परमात्मा के स्वरूप में साक्षात् संकोच-विकास नहीं हैं, परन्तु वे अपने शरीररूप जडाजड-संज्ञक दोनों प्रकृतियों में अन्तर्यामीरूप से स्वतः व्यापक होकर रहे हैं। इसीलिए, उन शरीरी परमात्मा में दोनों प्रकृतियों का संकोच-विकास उपचारमात्र होता है। यह भावार्थ समझना चाहिए। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 115 | 165 | १६५. अर्थ: “समस्त मनुष्यों के आत्मारूप भगवान सबमें अन्तःप्रवेश करके सबके शिक्षण प्रदाता तथा नियमन कर्ता बने हुए हैं।” (तैत्तिरीय आरण्यक: ३/११) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 115 | 166 | १६६. अर्थ: “जिस परमात्मा का ‘अक्षर’ शरीर है। वे समस्त भूतों के अन्तरात्मा हैं, निर्दोष हैं तथा दिव्य हैं। ऐसे एकमात्र देव नारायण हैं।” (सुबालोपनिषद्: ७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 115 | 167 | १६७. अर्थ: “जो परमात्मा जीवात्मा में अन्तःप्रवेश करके नियमन करते हैं, वे अन्तर्यामी तेरी अमृत आत्मा हैं, अर्थात् निरुपाधिक अमृतशाली परमात्मा हैं।” (बृहदारण्यक: ३/७/३०) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 115 | 168 | १६८. अर्थ के लिए देखें: वचनामृत गढ़डा प्रथम ५६ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 115 | 169 | १६९. मैं ब्रह्म हूँ (बृहदारण्यक: १/४/१०) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 118 | 170 | १७०. अर्थ: “ब्रह्मादि देव भी आपकी महिमा का पार नहीं पाते, क्योंकि आपकी महिमा अपार है। किंबहुना, आपने भी अपनी महिमा का अन्त नहीं पाया।” (श्रीमद्भागवत १०/८७/४१) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 118 | 171 | १७१. अर्थ: “जिस भक्त को भले ही शास्त्रज्ञान न हो परंतु दृढ़ विश्वासपूर्वक (मूढ़ रूप से) भगवान एवं संत के उपदेशानुसार भगवद्भजन करता है तथा जिस भक्त ने बुद्धि से परे रहनेवाले आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है वही ज्ञानी भगवान के सुख को प्राप्त करता है परंतु जो विश्वासी भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है ऐसा अंतरित भक्त हमेशा क्लेश प्राप्त करता है।” (श्रीमद्भागवत: ३/७/१७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 118 | 172 | १७२. अर्थ: “इन्द्रियों के आहार न करनेवाले मनुष्य की विषयवृत्ति आत्मा तक नहीं पहुँचती है। भक्त के लिए विषय निवृत्त हो जाते हैं। किन्तु उसकी आसक्ति निवृत्त नहीं होती। वह तो परमात्मा के साक्षात्कार से ही मिटती है।” (गीता: २/५९) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 118 | 173 | १७३. अर्थ: “सत्त्वगुण परब्रह्म का दर्शन करानेवाला है।” (श्रीमद्भागवत: १/२/२४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 118 | 174 | १७४. अर्थ: “हे उद्धव! विद्या तथा अविद्या मेरे शरीरभूत है। मेरी माया से निर्मित हुई है। उसमें विद्याशक्ति मोक्षदायिनी है तथा अविद्याशक्ति बन्धनकारी है।” (श्रीमद्भागवत: ११/११/३) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 119 | 175 | १७५. रामचरितमानस - बालकांड: ९४/५ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 120 | 176 | १७६. यहाँ सविकल्प-निर्विकल्प शब्द लौकिक अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ। किन्तु उपास्य स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में मायिक बुद्धि रखनेवाले को ‘सविकल्प निश्चयवाला’ है। और जिसे भगवत्स्वरूप में मायिक बुद्धि नहीं होती, वह निर्विकल्प निश्चयवाला है। निर्विकल्प निश्चय की उत्तरोत्तर अधिकता के अनुसार कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम भेद इस तरह दर्शाये गये हैं - कनिष्ठ निर्विकल्प निश्चयवाले को दस लोकों का नाश न हो, तब तक निश्चिय बना रहता है, लेकिन नैमित्तिक प्रलय में निश्चय नहीं रहता। मध्यम निर्विकल्प निश्चयवाले को श्वेतद्वीपादि धाम की स्थिति तक निश्चय रहता है, अर्थात् प्राकृत प्रलय तक निश्चय में स्थिरता रहती है; निर्विकल्प निश्चयवाला आत्यंतिक प्रलय में भी निर्विकार रहता है, उसका निश्चय कभी डिगता नहीं है। ऐसा भेद ‘सेतुमाला टीका’ में दर्शाया गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 121 | 177 | १७७. अर्थ: “ब्रह्मा द्वारा सृजित मरीच्यादि तथा उनके द्वारा उद्भूत कश्यपादिक तथा उनके द्वारा सृजित देवमनुष्यादि के मध्य इस लोक में नारायण ऋषि के सिवा ऐसा कौन-सा पुरुष है, जिसका मन स्त्रीरूपी माया से आकर्षित नहीं होता? अन्य समस्त मनुष्यों का मन ऐसी माया से आकर्षित हो ही जाता है।” (श्रीमद्भागवत: ३/३१/३७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 121 | 178 | १७८. अर्थ: “जिस प्रकार भगवान के भक्त का भगवत्स्वरूप सम्बंधी ज्ञान देह में रहनेवाले दोषों तथा जीव में स्थित अविद्यादि दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही परमेश्वर भी प्रकृति तथा जीववर्ग में व्याप्त होकर रहने के बावजूद प्रकृति के सत्त्वादि गुणों तथा जीव के अविद्या, अस्मिता एवं रागद्वेषादि दोषों से लिप्त नहीं होते। परमेश्वर की इतनी ही परमेश्वरता है, अर्थात् जब भक्त का भगवत्स्वरूप सम्बंधी ज्ञान, देहात्मा के दोष से लिप्त नहीं होता, तब जड तथा चैतन्य में अन्यर्यामी रूप से रहनेवाले भगवान जड या चेतन प्रकृति के दोषों से लिप्त न हों, इस विषय में कहने की बात ही क्या है?” (श्रीमद्भागवत: १/११/३८) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 121 | 179 | १७९. अर्थ: “जो मेरी ही शरण में आते हैं, वे मेरी गुणमयी तथा दुर्लंघ्य माया को पार कर लेते हैं।” (गीता: ७/१४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 121 | 180 | १८०. अर्थ: “मेरे साधर्म्य (समान गुण-योग) को प्राप्त किए हुए हैं।” (गीता: १४/२) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 121 | 181 | १८१. अर्थ: “हे नित्य, हे भगवन्, आप अपरिमित एवं सर्वव्यापक हैं। यदि असंख्य जीव आपकी तरह अपरिमित एवं सर्वव्यापक हो जाएँगे, तब तो वे आपके समान ही कहलाएँगे! फिर तो कौन नियामक तथा कौन नियम्य? यह (नियामक - नियम्य) तब ही स्थिर हो सकता है, जब आप ही नियामक हो। अन्यथा शाश्वत नियम का लोप हो जाए।” (श्रीमद्भागवत: १०/८७/३०) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 121 | 182 | १८२. छांदोग्योपनिषद्: ६/२/१ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 122 | 183 | १८३. जीवात्मा ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञान। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 122 | 184 | १८४. अर्थ: “मन अतिचंचल होता है, इस कारण उसकी स्थिति सदैव एकसमान नहीं रहती। इसलिए कभी भी इस पर ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि, ‘यह मेरे वश में हो चुका है। इसलिए अनर्थ नहीं करेगा।’ मन का विश्वास करने के कारण बड़े-बड़े सौभरि आदि ऋषियों का भी तप क्षीण हो गया था, जिसे सम्पादित करने के लिए उन्होंने दीर्घकाल तक महाप्रयास किए थे।” (श्रीमद्भागवत: ५/६/३) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 122 | 185 | १८५. अर्थ: “मन का विश्वास करनेवाले योगी का मन काम की पकड़ को सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर अवसर देता रहता है। योगी के मन में काम की पैठ को कोई मौका मिलने के बाद क्रोध आदि अन्तःशत्रुओं को भी वहाँ अपना आसन जमाने का अवसर मिल जाता है। जैसे पुंश्चली स्त्री विश्वास करनेवाले अपने पति का सफाया करने के लिए जार को मौका देती है, वैसे ही मन भी कामादि द्वारा योगी को पथभ्रष्ट कर डालता है।” (श्रीमद्भागवत: ५/६/४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 123 | 186 | १८६. शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान तथा श्रद्धा, ये अद्वैत वेदान्त में प्रसिद्ध ‘षट् संपत्ति’ हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 123 | 187 | १८७. महाभारत, शांतिपर्व: ३१६/४०, ३१८/४४ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 124 | 188 | १८८. अर्थ: “मेरे भय से वायु चलती है तथा मेरे भय से सूर्य प्रकाशित हो रहा है।” (श्रीमद्भागवत: ३/२५/४२) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 124 | 189 | १८९. पाठांतर: तुलसी जाके बदनत धोखेउ निकसत राम, ताके पगकी पगतरी मेरे तनुके चाम। (कल्याण, वर्ष: ३९, पृष्ठ: २४९) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 126 | 190 | १९०. श्रीमद्भागवत: १/१५/३४-३५ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 126 | 191 | १९१. अर्थ: “हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप वही चतुर्भुजरूप में हमें दर्शन दें।” (गीता: ११/४६) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 126 | 192 | १९२. अर्थ: “अपने किए हुए पापकर्मों के कारण मूढ़ पुरुष मेरे परमभाव को नहीं जानकर समस्त भूतों के महेश्वर तथा परम करुणापूर्वक सबके समाश्रय के लिए मनुष्यशरीर में स्थित मुझ भगवान की अवज्ञा करते हैं, अर्थात् वे मुझे प्राकृत मनुष्य तथा सजातीय मानकर मेरा तिरस्कार किया करते हैं।” (गीता: ९/११) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 128 | 193 | १९३. पूर्वापर सन्दर्भों का समन्वय करने से यहाँ ‘विषम भाव’ शब्द होना चाहिए। परंतु प्राचीनतम प्रतों में भी ‘समानता’ शब्द ही प्राप्य है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 128 | 194 | १९४. अर्थ: “यह समस्त जगत ब्रह्म-ब्रह्मात्मक है।” (छान्दोग्योपनिषद्: ३/१४/१) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 128 | 195 | १९५. अर्थ: “इस जगत में जो कुछ दृश्यमान है, सर्वत्र भगवान का निवास है, इसके बिना विविध पदार्थों का मानो अस्तित्व ही नहीं है।” (बृहदारण्यकोपनिषद्: ४/४/१९) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 128 | 196 | १९६. अर्थ: “यह समग्र विश्व भगवानरूप है, स्वरूप तथा स्वभाव से भगवान विश्व-विलक्षण हैं, तथापि भगवान से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, इसलिए जगत भगवान है, ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः भगवान विश्व से विलक्षण हैं।” (श्रीमद्भागवत: १/५/२०) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 128 | 197 | १९७. अर्थ के लिए देखिए: वचनामृत लोया ७ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 128 | 198 | १९८. अर्थ: “आत्माराम तथा रागद्वेषादिरूप ग्रन्थियों से रहित मुनि भी भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान में कारुण्य, सौशील्य एवं वात्सल्यादि गुण रहे हैं।” (श्रीमद्भागवत: १/७/१०) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 128 | 199 | १९९. अर्थ: “हे राजर्षे! सत्त्वादि गुणों के कार्यभूत तीन देहों से विलक्षण आत्मस्वरूप में सम्यक् रूप से निष्ठा प्राप्त करके भी मैं (शुक) उत्तमश्लोक भगवान की लीला से आकृष्ट होकर श्रीमद्भागवत को पढ़ चुका हूँ।” (श्रीमद्भागवत: २/१/९) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 129 | 200 | २००. अर्थ: “गुणातीत, ब्रह्मभावापन्न तथा स्वात्मस्वरूप में रहनेवाले मुनि भी भगवान के गुणानुवाद करते रहते हैं।” (श्रीमद्भागवत: २/१/७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 129 | 201 | २०१. अर्थ के लिए देखिए: वचनामृत पंचाला २ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 129 | 202 | २०२. अर्थ: “चार प्रकार के आर्तादि भक्तों में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सदैव मेरे साथ ही सम्बद्ध रहता है तथा एकमात्र मेरी ही भक्ति करता है। अवशिष्ट अन्य तीनों भक्त उसके सदृश नहीं हैं। तथा, ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय हैं और मैं उसे अत्यन्त प्रिय हूँ। यह तीन प्रकार के आर्तादि भक्त उदार (महान) हैं। परन्तु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही हैं, इस कारण वे मेरे लिए आत्मवत् प्रिय हैं, मैं ऐसा मानता हूँ।” (गीता: ७/१७-१८) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 130 | 203 | २०३. अर्थ: “मैं वैश्वानर (जठराग्नि) बनकर समस्त प्राणियों की देहों में रहता हूँ और प्राणियों द्वारा खाये गए चार प्रकार के अन्नों को प्राणापानवृत्ति से समायुक्त होकर पचाता हूँ।” (गीता: १५/१४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 130 | 204 | २०४. अर्थ: “हे जनार्दन! अब मैं आपके इस अतिसौम्य मनुष्यरूप के दर्शन करके स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हुआ हूँ।” (गीता: ११/५१) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 132 | 205 | २०५. अर्थ के लिए देखिए: वचनामृत लोया ७ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 132 | 206 | २०६. अर्थ के लिए देखिए: वचनामृत लोया ७ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 133 | 207 | २०७. अर्थ: “इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय परब्रह्म परमात्मा से होती है।” (श्रीमद्भागवत: १/१/१) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 133 | 208 | २०८. यहाँ ‘धाम’ शब्द भगवान के महात्म्य ज्ञानपरक कहा गया है। माया के अज्ञान को मिटाने का सामर्थ्य होने ‘धाम’ शब्द से ‘अक्षरब्रह्म’ अर्थ भी अपेक्षित है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 133 | 209 | २०९. अर्थ: “जो भक्त निष्कपट, अविच्छिन्न अनुवृत्ति से भगवान के चरणकमलों को भजता है, वह भक्त सर्वाधार, अपरिमित ऐश्वर्यवाले चक्रपाणि परमात्मा की पदवी को जानता है, अर्थात् उसको प्राप्त करता है।” (श्रीमद्भागवत: १/३/३८) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 133 | 210 | २१०. अर्थ के लिए देखिए वचनामृत लोया १८ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 133 | 211 | २११. अर्थ के लिए देखिए: वचनामृत गढडा प्रथम ४५ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 133 | 212 | २१२. श्रीमद्भागवत: ३/५/२६; परमात्मा ने पुरुषरूप से माया में वीर्य धारण किया। यहाँ मैथुनीभाव का रूपक ही दिया गया हैं, वास्तव में महाउत्पत्ति के समय स्त्री-पुरुष के आकार प्रकट न होने के कारण संकल्परूप वीर्य समझना चाहिए। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 134 | 213 | २१३. सूर्यसिद्धान्त १२/४३, ७४ तथा सिद्धान्तशिरोमणि मध्यमाधिकार, कालमान अध्याय: १३/१४ में दो ध्रुवों का वर्णन किया गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 134 | 214 | २१४. अर्थ: “विषयों के ध्याता पुरुष को विषयों में आसक्ति बढ़ती है, तब उसमें काम की उत्पत्ति हो जाती है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह पैदा हो जाता है। मोह से इन्द्रिय-विजय के लिए प्रारम्भ किए गए प्रयत्नों में सहायक स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है। स्मृतिभ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात् आत्मज्ञान के लिए किए गए प्रयासों का नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने से उसका विनाश हो जाता है, अर्थात् वह पुनः संसारचक्र में फँस जाता है।” (गीता: २/६२-६३) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 134 | 215 | २१५. अर्थ: “जिसको मिट्टी का पिंड, पत्थर और सुवर्ण तीनों समान हैं।” (गीता: १४/२४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 134 | 216 | २१६. अर्थ के लिए देखिए: वचनामृत पंचाला ३ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 134 | 217 | २१७. अर्थ के लिए देखिए: वचनामृत गढ़डा प्रथम १५ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 136 | 218 | २१८. अर्थ के लिए देखिए वचनामृत गढ़डा प्रथम १ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 139 | 219 | २१९. स्मृतिग्रंथ, गृह्यसूत्र तथा अन्य सदाचार प्रेरक ग्रंथ। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 141 | 220 | २२०. पद्मपुराण, उत्तर खण्ड: ३९/६७-१०५ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 141 | 221 | २२१. जहाँ अन्य टीकाकारों ने इसका अर्थ योगसाधना या व्रत-उपवास किया है, वहाँ भगवान स्वामिनारायण ने इसका अर्थ ब्रह्मरूप हो, परब्रह्म की उपासना कहा है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 141 | 222 | २२२. गीता (१५/७) तथा ब्रह्मसूत्र (२/३/४३) में जीवात्मा को अंशरूप कहा गया है, परंतु इस वचनामृत का निरूपण अन्य आचार्यों की अपेक्षा अत्यधिक तर्कशुद्ध एवं प्रेरक है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 141 | 223 | २२३. ‘ज्ञानयज्ञ’ का अर्थ अंतर्दृष्टि है तथा योगयज्ञ का अर्थ ‘अपनी इन्द्रियों तथा अंतःकरण को ब्रह्म-अग्नि में आहुति देना’ है। इस प्रकार दो अर्थ निकालने के बाद यहाँ दोनों को एक ही बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः योगयज्ञ रूप इन्द्रियों तथा अंतःकरण की ब्रह्म-अग्नि में आहुति देना भी एक प्रकार से ‘अंतर्दृष्टि’ ही है, तथा अंतर्दृष्टिरूप ‘ज्ञानयज्ञ’ भी इन्द्रियों तथा अंतःकरण को सत्पुरुष में जुड़ जाने का योगयज्ञ ही है। दोनों एक ही होने से यहाँ फलदर्शन के लिए ‘ज्ञानयज्ञ’ ही कहा जाएगा। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 141 | 224 | २२४. वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप सत्पुरुष में इन्द्रियाँ-अंतःकरण का होम करके अक्षरब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त कर भगवान की भक्ति-सेवा करना यही वचनामृत गढ़डा प्रथम ४०, वचनामृत लोया १२ आदि में उत्तम लक्ष्य मानकर स्वीकार किया है, उसी को यहाँ भी प्रधान ध्येय समझना चाहिए। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 142 | 225 | २२५. इन वचनों से श्रीहरि की सर्वोपरिता अर्थात् श्रीहरि दूसरें अवतारों से अलग एवं परे हैं, यह अत्यंत स्पष्ट समझा जाता है। अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी इस वचनामृत को पढ़कर अनेक बार ‘सर्वोपरिता’ का निरूपण करते थे। (३/१२) स्वामी कहते थे कि (७/१५) अक्षरादिक सभी से परे, और अद्वैतमूर्ति, जो प्रकट पुरुषोत्तम में तथा दूसरे विभूति अवतार में भेद किस प्रकार है? तो जैसे तीर तथा तीर को फेंकनेवाला, तथा चक्रवर्ती राजा तथा ख़िराज देनेवाले अन्य राजा, दोनों में अंतर है, तथा जैसे सूर्य एवं सूर्यमंडल के अन्य ग्रहों में अंतर है, उसी प्रकार इस प्रकट पुरुषोत्तम में एवं अन्य राम-कृष्णादिक अवतारों में अंतर है, इस प्रकार प्रकट पुरुषोत्तम को सर्वोपरि जानना। यही निरूपण स्वामी नित्यानंदजी (बात: १४) तथा विधात्रानन्दजी (बात: १४) ने किया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 142 | 226 | २२६. गीता: १८/६६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 142 | 227 | २२७. गीता: २/४० |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 143 | 228 | २२८. यहाँ ‘ब्रह्म’ शब्द वचनामृत गढ़डा प्रथम ४५ की तरह भगवान की अंतर्यामी शक्ति को निरूपित करता है, परंतु वह अक्षरधाम वाचक शब्द नहीं है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 143 | 229 | २२९. गीता: ४/९ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 144 | 230 | २३०. अर्थ: “हे सुव्रत! जिस प्रकार घृतादि वस्तुओं के अतिभक्षण से मनुष्यों में रोग उत्पन्न हो जाता है, उसका निवारण घृत द्वारा नहीं होता, बल्कि घृतादि वस्तुओं में औषधों को मिश्रित किया जाए, तो वे रोग का पूर्णतः मूलोच्छेद कर डालती हैं। वैसे ही मनुष्यों की समस्त क्रियाएँ (व्रत, यज्ञ, दानादि) अन्त में संसृति का कारण होती हैं। फिर भी, यदि वे ही क्रियाएँ परमेश्वर की भक्ति के रूप में की गई तो वे अनादि अज्ञान की निवृत्ति के साथ-साथ मोक्ष को भी सुलभ बना देती हैं।” (श्रीमद्भागवत: १/५/३३-३४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 144 | 231 | २३१. गीता: ४/१८ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 146 | 232 | २३२. अर्थ: “जिस ब्रह्मधाम को प्राप्त करके पुनः जन्म-मरण को भोगना नहीं होता तथा जिस धाम को सूर्य-चंद्र तथा अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, वही मेरा परम धाम है।” (गीता: १५/६) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 146 | 233 | २३३. भगवान स्वामिनारायण अक्षरातीत सर्वोपरि पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं से सभी अवतार प्रकट होते हैं, तथा पुनः उन्हीं में लीन होते हैं। जैसे तारे चन्द्र में लीन होते हैं, चन्द्र सूर्य में लीन होता है, उसी प्रकार लीनता समझना; परंतु जैसे जल में जल या अग्नि में अग्नि मिलती है, वैसे लीनता मत समझना। (गोपालानंद स्वामी की बातें: १/१७२) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 149 | 234 | २३४. अर्थ के लिए देखिए वचनामृत गढ़डा प्रथम १५ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 149 | 235 | २३५. गीता: ४/३९ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 150 | 236 | २३६. अर्थ के लिए देखिए वचनामृत गढ़डा मध्य ९ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 150 | 237 | २३७. यहाँ उल्लिखित ‘स्थितप्रज्ञता’ और गीताकथित ‘स्थितप्रज्ञता’ में अंतर है। गीता के दूसरे अध्याय में ‘आत्मनिष्ठा’ एवं सुख-दुःख में ‘समत्वभाव’ आदि को स्थितप्रज्ञता कहा गया है, जबकि यहाँ भगवत्स्वरूप के चरित्रों में मन की निश्चलता को स्थितप्रज्ञता कहते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 153 | 238 | २३८. अर्थ के लिए देखिए वचनामृत गढडा प्रथम प्रकरण ५० की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 154 | 239 | २३९. देखिए परिशिष्ट: ६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 164 | 240 | २४०. यहाँ ‘पुरुष’ विषयक विचार-विमर्श होने के कारण ‘पुरुष’ का उल्लेख किया गया है, वास्तव में यह चौथा अनादि तत्त्व ‘अक्षरब्रह्म’ ही है। (वचनामृत गढ़डा प्रथम ७) सत्संगिजीवन इत्यादि ग्रंथों में ‘पुरुष’ का कोई अनादि भेद नहीं कहा है। क्योंकि ‘पुरुष’ तो जीव तथा ईश्वर कोटि से आया हुआ मुक्तात्मा है; अतः वह अनादि भेद नहीं हो सकता। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | 172 | 241 | २४१. अर्थ के लिए देखिए वचनामृत पंचाला २ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 183 | 242 | २४२. श्रीहरि ने अक्षरब्रह्म के साथ इस प्रकार से अपनी आत्मा को विलीन करके रखा है, वह अन्य जीवों, ईश्वरों तथा अक्षरमुक्तों से भी उनका अक्षरब्रह्म के प्रति अनन्य प्रेम एवं एकता का सूचक है। अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के जीवनचरित्र में इस प्रकार की एकता की अनेक घटनाएँ उल्लिखित हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 187 | 243 | २४३. जिस पुरुष को वात, पित्त तथा श्लेष्मरूप त्रिधातुमय शरीर में आत्मबुद्धि है, स्त्री-पुत्रादि में ममत्वबुद्धि है तथा भूमि के विकारभूत प्रतिमादिक में पूजनीय देवताबुद्धि है और जल में तीर्थबुद्धि है, वैसी ही उस पुरुष की आत्मबुद्धि आदिक चारों बुद्धियाँ भगवान के एकान्तिक ज्ञानी भक्त में न हों तो उसे पशुओं में भी कनिष्ठ खर जानना चाहिए। (श्रीमद्भागवत: १०/८४/१३) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 188 | 244 | २४४. वर्तमान: जामनगर, गुजरात। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 190 | 245 | २४५. देखिए परिशिष्ट: ६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | 192 | 246 | २४६. कणभा गाँव के वैश्य भक्त। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 192 | 247 | २४७. डभाण के वैश्य भक्त। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | 192 | 248 | २४८. सुन्दरीयाणा के वणिक भक्त। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 192 | 249 | २४९. बोचासण के वैश्य भक्त। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 192 | 250 | २५०. सूरत के वणिक भक्त। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 192 | 251 | २५१. अहमदाबाद के वैश्य भक्त। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 199 | 252 | २५२. तथा करचरणादि अवयव रहित है तथा अणु के समान सूक्ष्म है। यही तात्पर्य है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 199 | 253 | २५३. अर्थात् शुकदेवजी आदि योगी ब्रह्मस्वरूप होने पर भी ब्रह्म में ही स्थिति पाकर संतुष्ट नहीं थे, परंतु भगवान की भक्ति ही किया करते थे। ऐसे वृत्तांत नहीं जानने के कारण ही योगियों को भगवान एवं संत के प्रति गौणभाव रहता है और आत्मदर्शन में अधिक रुचि रहती है। अतः योगियों को अपने पुरातन सन्तपुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 201 | 254 | २५४. सर्गः - महदादि पृथ्वीपर्यंत तत्त्वों की उत्पत्ति, अर्थात् वैराजपुरुष तक की सृष्टि। विसर्गः - ब्रह्मा द्वारा की हुई सृष्टि। स्थानम् - भगवान की सर्वोत्कृष्ट शत्रु – विजयादिरूप स्थिति। पोषणम् - जगत का रक्षणरूप भगवान का अनुग्रह। ऊतयः - कर्मवासना। मन्वन्तरकथाः - सद्धर्म, भगवान द्वारा अनुगृहीत मन्वन्तराधिपों का धर्म। ईशानुकथाः - भगवान के अवतारचरित्रों की कथा तथा उनके एकान्तिक भक्तों के नानाविध आख्यानों की सत्कथा। निरोधः - जीवसमुदाय का अपनी-अपनी कर्मशक्तियों के साथ सूक्ष्मावस्थावाली प्रकृति में रहना। मुक्तिः - तीन देह एवं तीन गुणों का त्याग करके अक्षरब्रह्म के साथ ऐक्यभाव प्राप्त करके परब्रह्म की सेवा करना। आश्रयः - जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होता है, श्रुति-स्मृतियाँ ‘परब्रह्म परमात्मा’ इत्यादि शब्दों से जिनकी महिमा-गान करती हैं, उनकी शरणागति। (श्रीमद्भागवत: २/१०/१) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 202 | 255 | २५५. यहाँ अक्षरधाम अर्थात् वैकुंठ धाम अथवा गोलोकधाम समझना चाहिए। क्योंकि पंचरात्र तंत्र की किसी संहिताओं में परमात्मा के उन धामों का उल्लेख ‘अक्षरधाम’ कहकर कहीं नहीं हुआ है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 202 | 256 | २५६. तथा वेदादि शास्त्रों का तात्पर्य साकार वासुदेव भगवान में ही है, इसीलिए। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 202 | 257 | २५७. वेदों में मुख्यतः नारायण ही प्रतिपादन है, अर्थात् वेद नारायण परक हैं, इन्द्रादि देवता भी नारायण के आधीन हैं, स्वार्गादि लोक के अधिपति भी नारायण ही हैं। यज्ञों द्वारा आराधना करने योग्य नारायण हैं। योग, तप, ज्ञान आदि साधनों द्वारा प्राप्य तत्त्व भी नारायण ही हैं। अतः इन सभी को नारायण परक ही समझना चाहिए। (श्रीमद्भागवत: २/५/१५-१६) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 202 | 258 | २५८. श्रीमद्भागवत: १/२/२८-२९ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 203 | 259 | २५९. यहाँ ‘वडवानल सदृश परम एकान्तिक साधु’ माया से परे स्थित अक्षरब्रह्मरूप सत्पुरुष का स्पष्टरूप से निर्देश करता है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 205 | 260 | २६०. अर्थ के लिए देखें, वचनामृत लोया १३ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 205 | 261 | २६१. गीता: १८/६६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 205 | 262 | २६२. संतों-भक्तों के समूह में रहकर आपसी प्रकृति-स्वभावों को या समस्याओं को सहन करने की साधना को श्रीहरि ‘भीड़ा’ शब्द से कहते थे। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 207 | 263 | २६३. अर्थ के लिए देखें, वचनामृत पंचाळा ७ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 210 | 264 | २६४. अर्थ आदि के लिए देखें, वचनामृत गढ़डा प्रथम ७७ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 211 | 265 | २६५. देखें परिशिष्ट: ६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 212 | 266 | २६६. नरसिंह महेता रचित भक्तिपद; देखें परिशिष्ट: ६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 212 | 267 | २६७. हे प्रभु! अहो! आश्चर्य की बात है कि ये वृक्ष, जिन्हें तमोगुण युक्त कर्म से ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है, देवताओं द्वारा पूजित आपके चरणारविंद की, मानो कि अपने तामसी कर्म के नाश के लिए पुष्प-फलादि सामग्री द्वारा पूजा कर रहे हैं! (श्रीमद्भागवत: १०/१५/५) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 215 | 268 | २६८. श्रीमद्भागवत: ३/१५/३४ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 215 | 269 | २६९. श्रीमद्भागवत: ७/१०/४३ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 217 | 270 | २७०. अज्ञानी तो केवल बिना कुछ समझे पंचविषयों में आकंठ डूबा रहता है, अतः उसमें तथा ज्ञानी में बड़ा अन्तर है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 218 | 271 | २७१. श्रीहरि स्वयं रामकृष्णादिक अवतारों के कारण अवतारी हैं, ऐसी स्पष्टता उन्होंने स्वयं वचनामृत गढ़डा मध्य ९, गढ़दा मध्य १३ आदि में की है। किन्तु मनुष्य शरीर धारी होने के कारण अन्य मुमुक्षुओं के हित के लिए वे स्वयं को श्रीकृष्ण के उपासक दिखाकर उनको अपने इष्टदेव कहते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 218 | 272 | २७२. इस वचनामृत में गोलोक के बीच अक्षरधाम का उल्लेख किया है, किन्तु इसका वर्णन वासुदेवमाहात्म्य (१७-१/२) तथा स्वामी की बातें (५-२८८) में किया गया है। उसके अनुसार गोलोकादिक अनंत धामों के बीच परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का अक्षरधाम सर्वोच्च है। परंतु यहाँ किया गया गोलोकधाम का उल्लेख पुरुषोत्तम नारायण के सर्वोपरि अक्षरधाम का नहीं है, ऐसा समझना। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 218 | 273 | २७३. अर्थ: “हे अर्जुन! पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष मेरे जन्म-कर्म को यथार्थरूप से दिव्य जानता है, वह पुरुष देहत्याग करने के पश्चात् फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझको ही प्राप्त कर लेता है।” (गीता: ४/९) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 218 | 274 | २७४. यहाँ ‘आप सभी का भगवान जो मैं’ ये शब्द भी श्रीहरि ने कहे थे, ऐसा गुरुपरंपरा के द्वारा ज्ञात होता है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 222 | 275 | २७५. अर्थात् ‘गुणातीत’ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 226 | 276 | २७६. अर्थ के लिए देखें: वचनामृत पंचाला २ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 226 | 277 | २७७. अर्थ: “भगवद्गुणों से आकृष्ट होकर मुनिवर्य शुकमुनि ने विष्णुजनों को प्रिय भागवत रूप महद् आख्यान की शिक्षा ली।”(श्रीमद्भागवत: १/७/११) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 226 | 278 | २७८. अर्थ के लिए देखें: वचनामृत पंचाला २ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 226 | 279 | २७९. अर्थ: “निर्गुणभाव को प्राप्त होने पर भी महान मुनिवर्य भगवान के चरित्रों का गान करते हैं।” (श्रीमद्भागवत: २/१/७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 226 | 280 | २८०. अर्थ के लिए देखें: लोया ७ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 228 | 281 | २८१. अर्थ: “हे भगवन्! कभी भी आपके नामों का श्रवण-कीर्तन करने, आपको प्रणाम करने तथा आपका स्मरण करने से यदि श्वपच तुरन्त यज्ञ करने में समर्थ और पवित्र हो जाता है, तो कोई प्राणी यदि आपके दर्शनमात्र से पवित्र और कृतार्थ हो जाए तो इसके सम्बंध में क्या कहना है! यह एक आश्चर्य की बात है कि श्वपच की जिह्वा पर भी आपका नाम बना रहता है और वह भी आपके नामोच्चार से भक्तिरहित कर्मठ ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाता है; तो जिन्होंने भगवान के नाम का उच्चार किया है, उन्हीं ने तप किया है, होम किया है, तीर्थ में स्नान भी उन्होंने ही किया है। तथा वे ही सदाचरणवाले हैं और वेदों का अध्ययन भी उन्होंने किया है।” (श्रीमद्भागवत: ३/३३/६-७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 228 | 282 | २८२. अर्थ: “समस्त जगत को सुख देनेवाली यह वायु मेरे भय से चलती रहती है, मेरे भय से ही सूर्य प्रकाश प्रदान करता रहता है, इन्द्र वर्षा करता रहता है, अग्नि वस्तुओं का दहन करती है तथा मृत्यु प्राणियों में विचरण करती रहती है।” (श्रीमद्भागवत: ३/२५/४२) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 233 | 283 | २८३. उक्त सम्प्रदाय में वृंदावन को ‘भगवद्धाम’ के रूप में विशेष माना गया है। (चैतन्य चरित्रामृत, आदि लीला: ५/१७-१९), मध्य लीला: २०/४०२, अत्यं लीला: १/६७) इसके उपरांत पद्मपुराण: ६९/६९, ७१ में कहा गया है कि वृंदावन नित्य है, प्रलयकाल में भी उस स्थान का विनाश नहीं होता। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 234 | 284 | २८४. वाल्मीकि रामायण: उत्तरकाण्ड: ४७/११-१२ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 243 | 285 | २८५. काल, कर्म तथा स्वभाव तीनों जीव के सुख-दुःख में निमित्तरूप हैं, उनमें। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 251 | 286 | २८६. अर्थ के लिए देखें: वचनामृत लोया १० की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 251 | 287 | २८७. यहाँ अंग्रेज गवर्नर का आदेश भारत देश के विभिन्न राजा, जो कि बड़े-बड़े स्टेट के सत्ताधीश थे, वे भी मानते थे, उस परिस्थिति का जिक्र करके दृष्टांत दिया गया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 251 | 288 | २८८. अर्थ: “अहो, गोपियाँ तो किसी के भी द्वारा त्याग न होनेवाली सम्बंधियों की तथा आर्यधर्म की मर्यादाओं का त्याग करके ऐसे भगवान की उपासना-भक्ति करने लगीं, जिन बालमुकुंद को वेद भी खोज रहे हैं! ऐसी गोपियों की चरणरज के स्पर्श से पुनित हुई लता, औषधि आदि के मध्य मैं भी कोई तृणगुच्छ बन जाऊँ, कि जिससे गोपियों की चरणरज के स्पर्श का मुझे भी लाभ प्राप्त हो...।” (उद्धवजी की प्रार्थना, श्रीमद्भागवत: १०/४७/६१) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 251 | 289 | २८९. अर्थ: “जो परमानन्द रूप है ऐसे सनातन, पूर्ण परब्रह्म श्रीकृष्ण जिनके मित्र है, ऐसे नंदगोप व्रजवासियों के अहोभाग्य हैं! जिनके भाग्य का वर्णन ही असंभव है।” (श्रीमद्भागवत: १०/१४/३२) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | 252 | 290 | २९०. जाबाल उपनिषद्: ४ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 254 | 291 | २९१. कवि सूरदास रचित भक्तिपद, देखें: परिशिष्ट: ६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 254 | 292 | २९२. स्वामी प्रेमानंदजी रचित भक्तिपद, देखें: परिशिष्ट: ६ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | 255 | 293 | २९३. अर्थ के लिए देखें: वचनामृत लोया १० की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | 256 | 294 | २९४. अर्थ के लिए देखें: वचनामृत लोया १३ की पादटीप। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 256 | 295 | २९५. अर्थ: “हे भगवान! जो आप ही को जीवन मानकर जीता है, उसके विपरीत जीवन जीनेवाले तो स्वयं के द्वारा परित्याग किए हुए विषयों से भी डरता रहता है। अर्थात् वासनामात्र से बंधनग्रस्त हो जाता है।” (श्रीमद्भागवत: ११/६/१७) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 262 | 296 | २९६. अर्थ: “ब्रह्मादि देव भी आपकी महिमा का पार नहीं पाते। क्योंकि आपकी महिमा अपार है, आप स्वयं आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते हैं। आप ऐसे महिमावंत हैं कि जिसके एक-एक रोम के छिद्र में अष्ट आवरणों से युक्त अनेक ब्रह्मांड विद्यमान हैं।” (श्रीमद्भागवत: १०/८७/४१) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 264 | 297 | २९७. परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के अनुप्रवेश से नरनारायण आदि ईश्वर ऐश्वर्य को प्राप्त करके अवतरित होते हैं। अतः पुरुषोत्तम नारायण और नरनारायण दोनों अत्यन्त भिन्न हैं। फिर भी सभा में उपस्थित भक्तों के जीव नरनारायण की प्रधानता होने से यहाँ दोनों की एकता कहते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | 266 | 298 | २९८. सर्वावतारी रूप से अपनी महिमा का निरूपण करके, श्रोताओं को पथ्य हो ऐसी हल्की सी बात करते हुए आगे कहते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 266 | 299 | २९९. सर्व अक्षरब्रह्म यानी ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त हुए अनंत मुक्त, उन मुक्तों से भी श्रेष्ठ भगवान के धामरूप जो अक्षरब्रह्म हैं, यानी कि मूर्तिमान अक्षर हैं, वह अनादि हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 266 | 300 | ३००. अक्षरधाम में बाग-बगीचा आदि का वर्णन भगवान के विशेष सामर्थ्य के रूप में समझना। वस्तुतः मुक्त को भगवान की मूर्ति के सिवाय ऐसे किसी पदार्थ या भोग की अपेक्षा या इच्छा नहीं है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 266 | 301 | ३०१. ‘गो’ यानी किरणें, ‘लोक’ यानी स्थान, गो + लोक = तेजोमय अक्षरधाम। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 267 | 302 | ३०२. यहाँ नरनारायण के मिष अपनी ही सर्वोपरिपन की महिमा दिखाते हैं, वह इस वाक्य में प्रयुक्त ‘प्रत्यक्ष श्रीनरनारायण’ शब्द से स्पष्ट रूप से मालूम होता है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 273 | 303 | ३०३. इस महाभारत के प्रसंग में पाठभेद दिखाई दे रहा है। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के साथ हुई घटना में राजकुमारों की कसौटी का प्रसंग जुड़ा हुआ है, जो कि पाण्डव, कौरव जब विद्यार्थी अवस्था में हस्तिनापुर में शस्त्रविद्या की शिक्षा ले रहे थे। जबकि मत्स्यवेध के समय द्रुपद के राजभवन में मत्स्यवेध की घटना साकार हुई थी, जहाँ द्रोणाचार्य उपस्थित नहीं थे। अतः इसे पाठभेद के रूप में देखना ही उचित है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 274 | 304 | ३०४. नरनारायण की ही महिमा जाननेवाले गुणभाविक भक्तों के लिए उनकी श्रद्धा बनी रहे, इस हेतु से श्रीहरि यहाँ अपने को नरनारायण स्वरूप से निरूपित करते हैं। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 112 | 305 | ३०५. श्रीमद्भागवत: ४/७/३०, ३/३१/३७, ६/१९/११ |